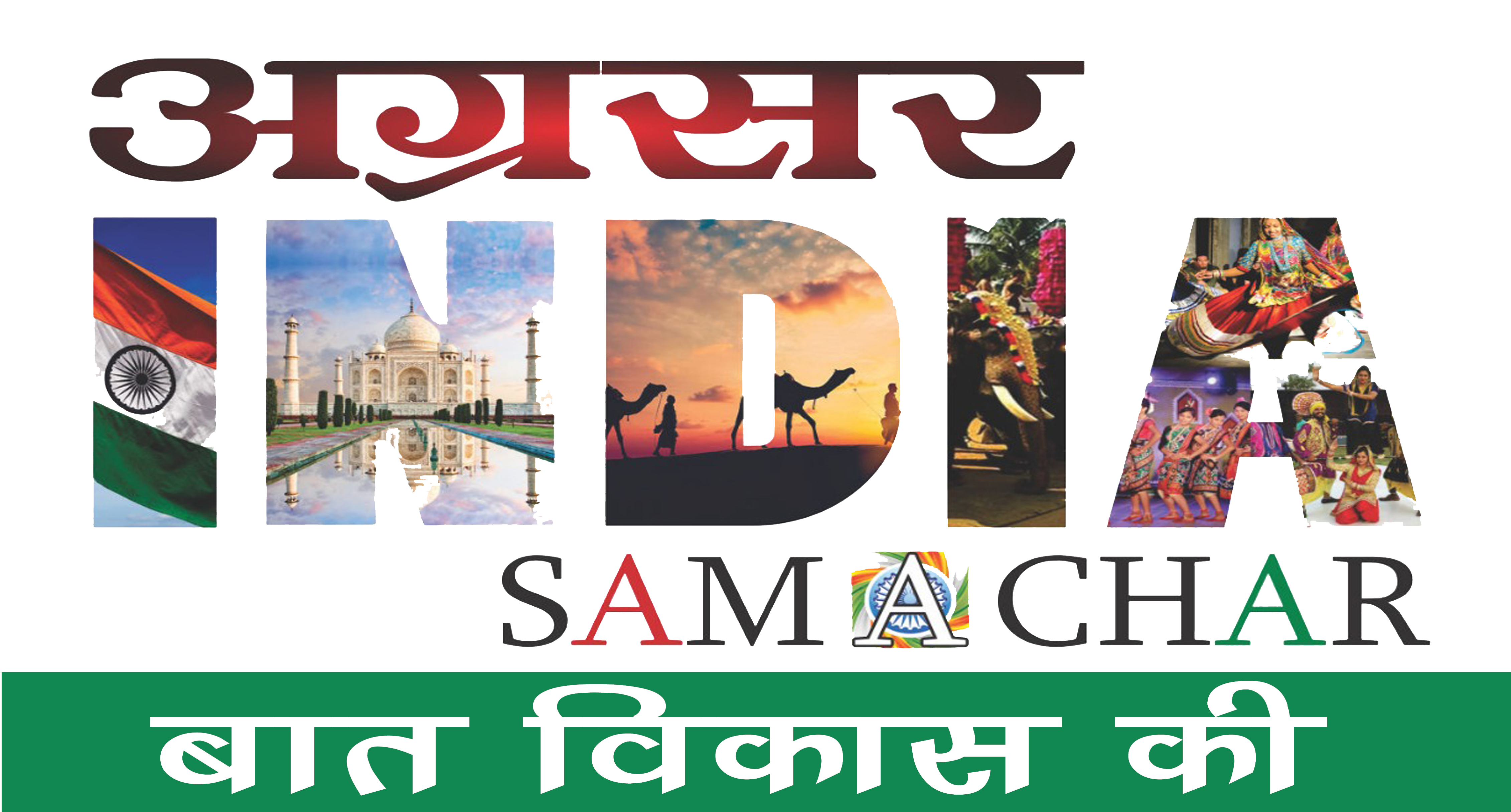नई दिल्ली: आज की पीढ़ी शायद उस खौफ और एकजुटता की कल्पना भी नहीं कर सकती, जो 54 साल पहले, 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पूरे देश में छाई हुई थी। शाम ढलते ही शहरों में पसरा सन्नाटा, घरों की बुझी हुई बत्तियां और कानों में गूंजते एयर रेड के सायरन – यह उस दौर की भयावह सच्चाई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तब ‘दुर्गा’ के रूप में उभरीं, जिनका नेतृत्व कठोर और निर्णायक माना गया।
1971 के युद्ध के दौरान, शाम होते ही पूरे देश में एक अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। लोगों को अपने घरों की बत्तियां बंद रखने की सख्त हिदायत थी, ताकि दुश्मन के विमान शहरों को पहचान न सकें। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले नागरिकों को एयर रेड से बचने के तरीके सिखाए गए थे – हमला होने पर कहां छिपना है और कैसे तुरंत बत्तियां बंद करनी हैं।
हर शहर में ब्लैकआउट, सड़कों पर घुप्प अंधेरा:
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर जैसे बड़े शहरों में रात के समय पूरी तरह से ब्लैकआउट किया जाता था। लोग गलती से भी अपने घरों की रोशनी नहीं करते थे। खिड़कियों पर काले पर्दे लगे रहते थे और स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जाती थीं, जिससे चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता था। हालांकि, कुछ ज़रूरी सार्वजनिक स्थानों पर रात के समय बहुत कम रोशनी की व्यवस्था की जाती थी।
कानों में गूंजते थे एयर रेड सायरन:
हर शहर में एयर रेड सायरन लगाए गए थे। जैसे ही हमले का खतरा होता, ये तेज़ आवाज़ वाले सायरन बज उठते थे, जो लोगों को तुरंत बंकरों या सुरक्षित स्थानों पर जाने का संकेत देते थे। ये सायरन आज भी कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में शिफ्ट बदलने की सूचना देते हैं, लेकिन 1971 में इनकी आवाज़ में खतरे का एहसास घुला होता था।
सीमावर्ती इलाकों में बंकर और खाली होते गांव:
अमृतसर, जम्मू और श्रीनगर जैसे सीमावर्ती शहरों में ज़मीन के नीचे सुरक्षित बंकर बनाए गए थे, जो बम के हमलों से बचाव कर सकते थे। युद्ध के दौरान पंजाब, राजस्थान, जम्मू और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों के कई गांवों को बड़े पैमाने पर खाली करा लिया गया था।
सूचना का एकमात्र सहारा – रेडियो:
54 साल पहले, 1971 में लोगों के लिए सूचना का मुख्य स्रोत रेडियो ही था। ऑल इंडिया रेडियो (AIR) युद्ध की हर खबर, सरकारी घोषणाएं और देशभक्ति के गीतों का प्रसारण करता था। बड़े शहरों में अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए विशेष नियंत्रण केंद्र बनाए गए थे। आज के दौर में सूचना के अनगिनत माध्यम हैं, लेकिन तब रेडियो ही एकमात्र सहारा था, जिस पर लोग हर पल युद्ध की खबरें जानने के लिए निर्भर रहते थे। अखबार तो अगले दिन सुबह ही आता था।
सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम:
सैन्य ठिकानों, रेलवे स्टेशनों, तेल रिफाइनरियों, बंदरगाहों और बड़े कारखानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। रात के समय रेलगाड़ियां बिना हेडलाइट के चलती थीं और सिग्नल के माध्यम से एक-दूसरे से संपर्क बनाए रखती थीं। रात में यात्री विमानों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। कई फैक्ट्रियों को छलावरण वाले पर्दों और रंगों से ढक दिया गया था ताकि वे दुश्मन के हवाई हमलों से बच सकें।
शहरों में तनाव और देशभक्ति का ज्वार:
युद्ध का तनाव हर तरफ और हर चेहरे पर साफ दिखाई देता था। लोग भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन अखबारों की बिक्री आसमान छू रही थी, क्योंकि हर कोई युद्ध से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर जानना चाहता था। इसके साथ ही, पूरे देश में देशभक्ति का एक जबरदस्त माहौल भी था। डर के साथ-साथ देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा लोगों में हिलोरे मार रहा था।
हर गली-मोहल्ले में ‘जय हिंद’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे गूंजते थे और देशभक्ति के पोस्टरों से दीवारें रंगी होती थीं। नागरिक बढ़-चढ़कर रक्तदान शिविरों और सैनिक परिवारों की सहायता के लिए आयोजित शिविरों में हिस्सा ले रहे थे।
पेट्रोल और खाने-पीने की चीजों पर राशनिंग:
1971 का दौर देश में अभावों का दौर था। पेट्रोल, केरोसीन, अनाज और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर राशनिंग लागू कर दी गई थी। बड़े शहरों में खाने-पीने की चीजों के लिए लंबी-लंबी कतारें लगती थीं, हालांकि स्थिति कभी इतनी खराब नहीं हुई कि लोग भूखे रहें। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ होने और भारत पर आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी के कारण आयात पर असर पड़ा था। उस समय तक भारत खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था और उसी साल वैश्विक तेल संकट ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया था। इस वजह से सरकार को वाहनों के लिए पेट्रोल की राशनिंग करनी पड़ी थी, जिससे बसों और निजी वाहनों का चलना कम हो गया था और लोग साइकिल या पैदल चलने पर मजबूर हो गए थे।
वनस्पति घी और रिफाइंड तेल की भी कमी हो गई थी, क्योंकि इनका आयात होता था। चीनी का उत्पादन कम होने और वितरण प्रणाली अस्त-व्यस्त होने से राशन कार्ड के जरिए इसका वितरण किया गया। गेहूं और चावल की भी कमी के कारण राशन की दुकानों से सीमित मात्रा में अनाज मिलता था। राशन की दुकानों पर लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था और चीनी, तेल और पेट्रोल जैसी चीजों के लिए हाथापाई तक की नौबत आ जाती थी।
हालांकि, ऐसा नहीं था कि सभी लोग देशभक्ति से ओतप्रोत थे। उस दौर में कुछ व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं को छिपाकर महंगे दामों पर बेचा और कालाबाजारी की, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हुई। कपड़ा उद्योग भी प्रभावित हुआ, जिससे कपड़ों की उपलब्धता कम हो गई। इन अभावों ने हालांकि बाद में भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद हरित क्रांति और तेल उत्पादन में स्वदेशी स्वावलंबन को बढ़ावा मिला।
रेडियो और देशभक्ति फिल्मों का बोलबाला:
उस दौर में टेलीविजन का प्रसार नहीं था। मनोरंजन और सूचना का मुख्य साधन रेडियो और फिल्में थीं। देशभक्ति का जबरदस्त उभार हुआ था। लता मंगेशकर का ‘ए मेरे वतन के लोगों’ एक बार फिर से लोकप्रिय हो गया था, सिनेमाघरों में युद्ध पर आधारित फिल्में दिखाई जाती थीं और ऑल इंडिया रेडियो से देशभक्ति के गीत लगातार प्रसारित होते थे। लोगों की सबसे ज्यादा निर्भरता रेडियो पर थी, जो लगातार युद्ध के बुलेटिन सुनाता था, जिससे उन्हें लड़ाई की हर जानकारी मिलती रहती थी। कवि, लेखक और कलाकारों ने देशभक्ति गीत, कविताओं और नाटकों के जरिए लोगों को प्रेरित किया।
हालांकि, उस दौर में अफवाहें भी खूब फैलती थीं। कभी दिल्ली पर हवाई हमले की झूठी खबर फैल जाती थी तो कभी परमाणु बम की धमकी की बातें होती थीं।
पूरी रात रेडियो से चिपके रहे लोग:
4 दिसंबर 1971 की रात जब भारतीय नौसेना ने ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’ में कराची बंदरगाह पर हमला किया, तो मुंबई में तुरंत ब्लैकआउट कर दिया गया। लोग पूरी रात रेडियो के आगे बैठे रहे, यह जानने के लिए कि क्या कराची पर हमला सफल रहा।
मॉक ड्रिल और नागरिकों की भागीदारी:
स्कूलों और कॉलेजों में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल करवाई जाती थी। बच्चों को सायरन की पहचान सिखाई जाती थी। रिटायर्ड सैनिकों और एनसीसी कैडेटों को शहरों में मदद के लिए तैनात किया गया था। लोगों ने बढ़-चढ़कर रक्तदान किया और सैनिक परिवारों के लिए राहत सामग्री इकट्ठा की।
1971 का युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह पूरे देश की एकजुटता, देशभक्ति और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने के जज्बे का प्रतीक था। इंदिरा गांधी का दृढ़ नेतृत्व और देशवासियों का अटूट समर्थन इस युद्ध में भारत की विजय का आधार बना।